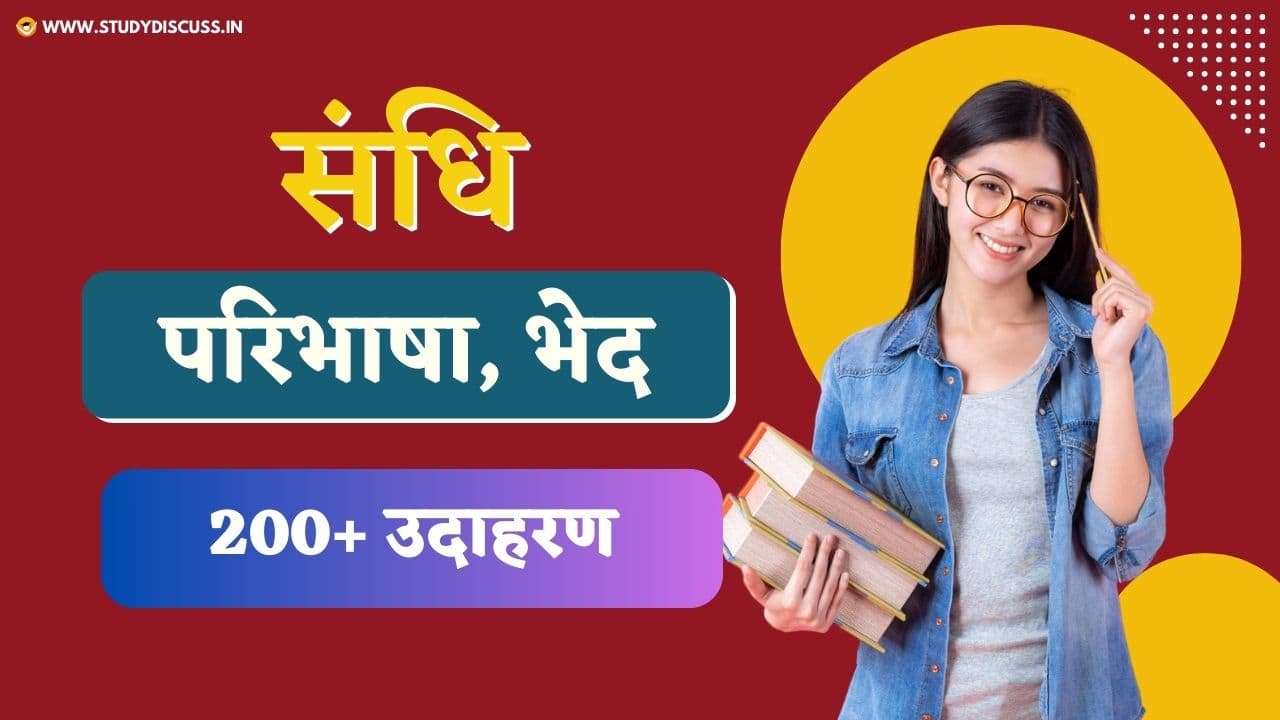
संधि (Sandhi) एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योकि हिंदी भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण में संधि की परिभाषा (Sandhi Ki Paribhasha) को पढ़ना बहुत जरुरी है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओ पीएससी, बैंकिंग, शिक्षक भर्ती (सीटीईटी, केवीएस, डीएसएसबी) आदि में चार से पांच प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जैसे कि संधि (Sandhi Ki Paribhasha) किसे कहते हैं? संधि के प्रकार (Sandhi Ke Prakar), संधि विच्छेद (Sandhi Vichchhed in Hindi), संधि से सम्बंधित अपवाद इत्यादि। इस पोस्ट में हम संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
संधि की परिभाषा (Sandhi Ki Paribhasha)
संधि की परिभाषा : सधि संस्कृत का शब्द है इसका सामान्य अर्थ “मेल” होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार(परिवर्तन) को संधि कहते हैं।
या
संधि की परिभाषा (Sandhi Ki Paribhasha) – जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते है तब जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं।
संधि विच्छेद किसे कहते हैं (Sandhi Vichchhed in Hindi)
संधि किये गये शब्दों को अलग-अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद (Sandhi Vichchhed in Hindi) कहलाता है।
उत्पत्ति: दो शब्द जब एक दूसरे के पास होते है, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक-दूसरे से मिल जाते हैं।
इसे भी पढ़े – रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव
संधि के गुण:
- संधि में दो वर्णों का मेल होता है।
- संधि संस्कृत भाषा की देन है।
- संधि में समास नहीं होता है, किन्तु समास में संधि होता है।
- संधि का निर्माण तत्सम शब्दों से होता है।
- संधि में अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है।
संधि के उदाहरण:
| संधि विच्छेद | संधि |
|---|---|
| रमा + ईश | रमेश |
| मत + अनुसार | मतानुसार |
| धर्म + अर्थ | धर्मार्थ |
| आशी: + वचन | आशीर्वचन |
| जगत् + जननी | जगज्जननी |
संधि के प्रकार (Sandhi Ke Prakar)
संधि के प्रकार (Sandhi Ke Prakar) मुख्य रूप से तीन हैं, जिसे हमने निचे विस्तार से समझाया है। जिसमे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ-साथ अपवाद को भी बताया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं साथ ही साथ इससे बनने वाले अभ्यास प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। संधि के प्रकार में सबसे पहले स्वर संधि आता है इसके भी पांच प्रकार होते हैं।
स्वर संधि
दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो, स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन(विकार) होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं।
- धर्म + अर्थ = धर्मार्थ
- विद्या + आलय = विद्यालय
- महा + आत्मा = महात्मा,
- महा + आनन्द = महानन्द
स्वर संधि के भेद
संधि में वैसे तो सभी संधि मुख्य हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाये तो स्वर संधि से अधिक सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि स्वर संधि के भी पांच प्रकार (स्वर संधि के भेद) के होते हैं जो निम्न है।
- दीर्घ स्वर संधि
- गुण स्वर संधि
- वृद्धि स्वर संधि
- यण स्वर संधि
- अयादि स्वर संधि
दीर्घ स्वर संधि
यदि किसी स्वर को उसके सवर्ण (सजातीय) स्वर के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो स्वर बनेगा वह दीर्घ स्वर होगा। अर्थात् हस्व या दीर्घ ‘आ’, ‘इ’, ‘उ’, के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ ‘आ’, ‘इ’, ‘उ’ स्वर आएं तो दोनों को मिलकर आ, ई, ऊ (दीर्घ ) हो जाते है।
| अ + अ = आ | अ + आ = आ |
| आ + अ = आ | आ + आ = आ |
| इ + इ = ई | इ + ई = ई |
| ई + इ = ई | ई + ई = ई |
| उ + उ + ऊ | उ + ऊ = ऊ |
| ऊ + उ = ऊ | ऊ + ऊ = ऊ |
| ऋ + ऋ = ऋ | – |
सवर्ण के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण होता है।
| अ + अ = आ | धर्म + अर्थ = धर्मार्थ दैत्य + अरि = दैत्यारि वीर + अगंना = विरांगना लोक + अर्पण = लोकार्पण पर + अधीन = पराधीन मत + अनुसार = मतानुसार |
| अ = आ = आ | भोजन + आलय = भोजनालय नव + आगत = नवागत राम + आश्रय = रामाश्रय |
| आ + अ = आ | यथा + अर्थ = यथार्थ शिक्षा + अर्थी = शिक्षार्थी तथा + अपि= तथापि |
| आ + आ = आ | विद्या + आलय = विद्यालय महा + आत्मा = महात्मा महा + आनन्द = महानन्द महा + आशय = महाशय |
| इ + इ = ई | वारि + इन्द्र = वारीन्द्र कपि + इन्द्र = कपिन्द्र कवि + इन्द्र = कवीन्द्र रवि + इन्द्र = रवीन्द्र अति + इव = अतीव |
| इ + ई = ई | कवि + ईश्वर = कवीश्वर हरि + ईश = हरीश परि + ईक्षा = परीक्षा गिरि + ईश = गिरीश |
| ई + इ = ई | मही + इन्द्र = महीन्द्र देवी + इच्छा = देवीच्छा |
| ई + ई = ई | जानकी + ईश = जानकीश नदी + ईश = नदीश रजनी + ईश = रजनीश नारी + ईश्वर = नारीश्वर |
| उ + उ = ऊ | भानु + उदय = भानूदय विधु + उदय = विधूदय सु + उक्ति = सूक्ति |
| उ + ऊ = ऊ | लघु + ऊर्मी = लघूर्मि साधू + ऊर्जा = साधूर्जा |
| ऊ + उ = ऊ | भू + उपरि = भूपरि गुरू + उपदेश = गुरूपदेश |
| ऊ + ऊ = ऊ | भू + ऊर्जा = भूर्जा भू + उद्धार = भूद्वार भू + ऊष्मा = भूष्मा |
| ऋ + ऋ = ऋ | पितृ + ऋण = पितृण मातृ + ऋण = मातृण |
गुण स्वर संधि
यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘इ’ या” ई, ‘उ’ या ‘ऊ’ तथा ‘ऋ’ स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते है।
| अ + इ = ए | देव + इन्द्र = देवेन्द्र भारत + इंदु = भारतेन्दु उप + इन्द्र = उपेन्द्र |
| अ + ई = ए | दुर्ग + ईश = दुर्गेश सुर + ईश = सुरेश |
| आ + इ = ए | यथा + इष्ट = यथेष्ट महा + इन्द्र = महेंद्र |
| आ + ई = ए | महा + ईश = महेश उमा + ईश = उमेश |
‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘उ’ या ‘ ऊ’ आए तो दोनों के मेल से ‘ओ’ हो जाता है
| अ + उ = ओ | पर + उपकार = परोपकार सूर्य + उदय = सूर्योदय |
| अ + ऊ = ओ | जल + ऊर्मि = जलोर्मि समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मी |
| अपवाद | प्र + ऊढ़ = प्रौढ़ |
| आ + उ = ओ | गंगा + उदय = गंगोदय महा = उत्सव = महोत्सव |
वृद्धि स्वर संधि
- अ/आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मिलने से ‘ऐ’ हो जाता है।
- अ या आ के बाद ओ या औ के आने से दोनों मिलकर ‘औ’ का निर्माण करते है।
| अ + ए = ऐ | एक + एक = एकैक लोक + एषण = लोकैषणा तत्र + एव = तत्रैव |
| अ + ऐ = ऐ | परम + ऐश्वर्य = परमैश्वर्य धन +ऐश्वर्य = धनैश्वर्य मत + ऐक्य = मतैक्य |
| आ + ए = ऐ | तथा + एव = तथैव सदा + एव = सदैव |
| आ + ऐ = ऐ | महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य रमा + ऐश्वर्य = रमैश्वर्य |
| अ + ओ = औ | वन + ओषधि = वनौषधि |
| अ + औ = औ | वन + औषध = वनौषध परम + औदार्य =परमौदार्य |
| आ + औ = औ | महा + औदांर्य = महौदार्य महा + औषधि = महौषधि महा + ओज = महौज |
यण स्वर संधि
यण स्वर संधि में इ, ई के बाद इ, ई, को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो इ, ई, के स्थान पर ”य” हो जाता हैं एवं उ, ऊ, के बाद उ, ऊ, को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उ, ऊ, के स्थान पर ‘व’ हो जाता है।
| इ + अ = य | यदि + अपि = यद्यपि अति + अंत = अत्यंत अधि + अयन = अध्ययन |
| इ + आ = या | इति + आदि = इत्यादि नि + आय = न्याय अति + आचार = अत्याचार |
| इ + उ = यु | अति + उत्तम = अत्युत्तम उपरि + उक्त = उपर्युक्त |
| इ +ऊ = यू | नि + ऊन = न्यून वि + ऊह = व्यूह |
| इ + ए = ये | प्रति + एक = प्रत्येक अधि + एषणा = अध्येषणा मति + एक = मत्येक |
| इ + ऐ = ये | अति + ऐश्वर्य = अत्यैश्वर्य |
| ई + अ = य | नदी + अर्पण = नध्यर् |
| ई + ऊ = यू | वाणी + ऊर्जा = वान्यूर्जा |
| उ + आ = व | सु़ + आगत = स्वागत मधु + आलय = मध्वालय |
| ऋ + अ = र | पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा मातृ + आज्ञा = मात्राज्ञा |
अयादि स्वर संधि
ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर (अर्थात् ए, ऐ, ओ, औ) को छोड़कर कोई अन्य स्वर आये तो उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं।
- ‘ए’ के स्थान पर अय हो जाता है।
- ‘ऐ’ के स्थान पर आय हो जाता है।
- ‘ओ’ के स्थान पर अव हो जाता है।
- ‘औ’ के स्थान पर आव हो जाता है।
| ए + अ = अय | चे + अन = चयन ने + अन = नयन शे + अन = शयन |
| ऐ + अ = आय | गै + अक = गायक शै + अर = शायर |
| ऐ + इ = आयि | शै + इका = शायिका दै + एनी = दायिनी |
| ओ + अ = अव | पो + अन = पवन हो + अन = हवंन |
| ओ + इ = अवि | पो + इत्र = पवित्र |
| ओ + ई = अवी | गो + ईश = गवीश |
| औ + अ = आव | पौ + अक = पावक |
| औ + इ = आवि | नौ + इक = नाविक |
| औ + उ = आवु | भौ + उक = भावुक |
व्यंजन संधि
वह संधि जिसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ‘व्यंजन’ होता है उसे व्यंजन संधि कहते है। दूसरे शब्दों में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आये तो उनके मिलने से जो विकार(परिवर्तन) होता है उसे व्यंजन सन्धि कहते है। व्यंजन संधि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है।
इसे भी पढ़े – विराम चिन्ह के प्रकार, प्रयोग और नियम
व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम
(अ). यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्पर्श व्यजन वर्ग का पहला वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्,) तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर या किसी भी वर्ग का व्यंजन( पंचम वर्ग को छोड़कर ) हो तो पहले वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ण के तीसरा वर्ण (ग्, ज्, ढ्, ब्) में बदल जाता है। अर्थात्
| क् का ग् होना | दिक् + गज = दिग्गज वाक् + ईश = वागीश |
| च् का ज् होना | अच् + आदि = आजादि |
| ट् का ड् होना | षट् + आनन = षडानन |
| त् का द् होना | जगत् + ईश = जगदीश सत् + आचार = सदाचार |
| प् का ब् होना | अप् + ज = अब्ज |
(ब). यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण तथा अंतिम वर्ण यदि अनुनासिक या पंचम वर्ण हो तो पहले के स्थान पर उसी वर्ग का पाचवा वर्ण में बदल जाता है। अर्थात्
| क् का ड् का होना | वाक् + मय = वाङ्मय |
| च् का ञ का होना | रुच् + मय = रुञमय |
| ट् का ण होना | षट् + मुख = षण्मुख |
| त् का न होना | उत् + नयन = उन्नयन |
| प् का म होना | अप् + मय = अम्मय |
(स). ‘म’ का नियम: यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म् हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का कोई व्यंजन (क से म तक) हो तो म् उसी वर्ग के पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है।
- सम् + धि = संधि
- सम् + कल्प = संकल्प
- सम् + भाग = संभाग
- सम् + कीर्ण = संकीर्ण
(द). यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म् हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अन्तस्थ( य, र, ल, व् ) या ऊष्म (ष, श, स, ह,) हो तो संधि के समय ‘म’ के स्थान पर अनुस्वार उच्चारण होता है।
- सम् + यम = संयम
- सम् + योग = संयोग
- सम् = न्यासी = सन्यासी
(इ). यदि ‘म’ के बाद ‘म’ ए तो ‘म’ अपरिवर्तित रहता है।
- सम् + मान = सम्मान
- सम् + मुख = सम्मुख
- सम् + मेलन = सम्मलेन
(उ). यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ‘त्’ तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ‘च’ हो तो ‘त्’ एवं च मिलकर च्च के रूप में उच्चारित होता है।
| त् + च = च्च | उत् + चारण = उच्चारण सत् + चरित्र = सच्चरित्र |
| त् + ज = ज्ज | सत् + जन = सज्जन |
| त् + ल = ल्ल | उत् + लास = उल्लास |
| त् + श = च्छ | उत् + श्वास = उच्छ्वास |
विसर्ग संधि
किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते है।
इसे भी पढ़े – काल (Tense) के प्रकार, नियम और उदाहरण
विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम
(1). विसर्ग (:) का परिवर्तन न होना – यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ के साथ विसर्ग (:) हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नही होता है।
- प्रातः + काल = प्रातःकाल
- पुनः + प्राप्ति = पुनःप्राप्ति
- पुनः + फलित = पुनःफलित
नम: + कार = नमस्कार
पुरः + कार = पुरस्कार
तिरः + कार = तिरस्कार
(2). विसर्ग का श् में परिवर्तन – यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग तथा शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो तो विसर्ग श् में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात् विसर्ग (:) + च, छ = विसर्ग का श् में परिवर्तन
- निः + चल = निश्चल
- निः + चय = निश्चय
- दु: + चरित्र = दुश्चरित्र
(3). विसर्ग का ष् में परिवर्तन – यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग तथा शब्द का प्रथम वर्ण ट या ठ हो तो विसर्ग ष् में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात् विसर्ग (:) + ट, ठ = विसर्ग का ष् में परिवर्तन
- धनु: + टंकार = धनुष्टंकार
- दु: + ट = दुष्ट
(4). विसर्ग का स् में परिवर्तन – यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग तथा शब्द का प्रथम वर्ण त या थ हो तो विसर्ग स् में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात् विसर्ग (:) + त, थ = विसर्ग का स् में परिवर्तन
- नम: + ते = नमस्ते
- निः + तार = निस्तार
(5). विसर्ग का परिवर्तन र् होना – यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर या स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अन्तस्थ (य, र, ल, व्) हो तो विसर्ग के स्थान पर र् का उच्चारण किया जाता है।
- दु: + आत्मा = दुरात्मा
- दु: + जन = दुर्जन
- नि: + अर्थक = निरर्थक
पुन: + गठन = पुनर्गठन
पु: + जन्म = पुनर्जन्म
स्व: + ग = स्वर्ग
अधिक पूछे जाने वाले सवाल
संधि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं?
संधि का अर्थ है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन। यह वर्णों के मेल से नए शब्द का निर्माण करती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है – स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि के कितने भेद हैं?
स्वर संधि मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं- दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि।
व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है?
व्यंजन संधि में व्यंजन के मेल या परिवर्तनों से नए शब्द का निर्माण होता है जिसके कुछ उदाहरण हैं
भवत् + भक्ति = भवद्भक्ति, सप्त + अर्षि = सप्तर्षि, शब्द् + कृत = शाब्दकृत, जगत् + नाथ = जगन्नाथ, सत् + गुण = सद्गुण, तत् + त्व = तत्त्व, लक्ष्मि + ईश = लक्ष्मीश
विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है?
विसर्ग संधि में विसर्ग (ः) का मेल अन्य स्वर या व्यंजन से होता है, जिससे ध्वनि में परिवर्तन होता है।
उदाहरण – योगः + च = योगश्च, राजः + ऋषि = राजर्षि, दुः + ख = दुःख, प्रियः + इव = प्रियतिव, निः + चल = निश्चल, निः + चय = निश्चय, दु: + चरित्र = दुश्चरित्र
- आखिरी अपडेट: 4 मिनट पहले
हमें आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया इस लेख के बारे में अपने विचार और सुझाव हमें बताएं। अधिक जानकारी पढ़ते रहने और नई अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो और सब्सक्राइब करें।




